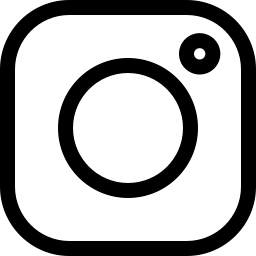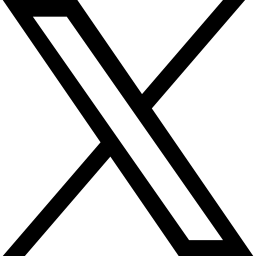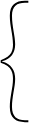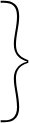-डॉ. दादूराम शर्मा*
अर्थ या धन मानव जीवन का आधार है । हमारे मनीषियों ने प्राचीन काल में जिन चार पुरुषार्थों की स्थापना की थी, वे हैं– धर्म अर्थ, काम और मोक्ष । विज्ञान के इस युग ने धर्म और मोक्ष की मान्यताओं को पूरी तरह नकार दिया है अथवा संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। फलतः मानव की सम्पूर्ण सत्ता उसके भौतिक पिंड में सिमटकर रह गई है। ऐसी स्थिति में अर्थ का प्रधान हो जाना स्वाभाविक ही है, क्योंकि उसी पर हमारी समस्त कामनाओं की पूर्ति निर्भर है। फिर भी मनुष्य यदि स्वयं को जीविका–पूर्ति या अपनी रोटी, कपड़ा और मकान तक सीमित रखता तो गनीमत थी, किंतु जब उसके मन में ‘तृष्णा’ (असीमित और अनियंत्रित भोग- लालसा) ने जन्म लिया तो उसमें उनके साधन भूत धन को बटोरने की प्रबल इच्छा ‘वित्तैषणा’ जागृत हो गई और यहीं से प्रारंभ हुई मानव जगत में भयानक संघर्ष की कहानी ।
हमारी इच्छाएं असीम हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है; दूसरी पूरी होती है तो तीसरी उत्पन्न हो जाती है। इन अनंत लालसाओं की पूर्ति के लिए हमें असीमित धन भी चाहिए। धन कमाने का आदिम उपाय है– ‘श्रम’ । श्रम दो तरह का होता है– शारीरिक और मानसिक या बैद्धिक । शारीरिक श्रम से आदमी किसी तरह पेट भरने लायक ही धन कमा सकता है और मानसिक श्रम से भी उसे पर्याप्त धन तो मिल सकता है किंतु उतना नहीं, जिससे वह अपनी नित्य बढ़ने वाली भोग- लालसाओं की पूर्ति कर सके । अतः उसने त्वरित धन प्राप्ति के अन्य बेहतर और कारगर उपायों पर विचार किया, जिनमें सर्वप्रमुख था परद्रव्यापहार बल से अथवा छल से दूसरों का धन हड़प लेना। बल से, लूट या युद्ध द्वारा या छल से, ठगी, धोखाधड़ी अथवा जुए आदि द्वारा आदमी आदिम युग से ही दूसरों का धन हड़पता आया है ।
बीसवीं सदी के तथाकथित सभ्य मानव ने प्रचुर धन प्राप्ति का एक अभिनव उपाय खोज निकाला, जिसे ‘भ्रष्टाचार’ या ‘करप्शन’ कहा जाता है । वाणिज्य – व्यापार में भ्रष्टाचार जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाज़ारी, तस्करी आदि के रूप में व्याप्त हो गया, तो नेताओं और अधिकारियों में वह रिश्वतखोरी है और कर्मचारियों में रिश्वतखोरी के साथ-साथ टालमटोली और कामचोरी | ‘दहेज-प्रथा’ और ‘दहेज प्रताड़ना’ भी इसके सामाजिक रूप हैं।
समाज में सर्वत्र धन और साधन सम्पन्नता का सम्मान हो रहा है। आज ‘व्यक्ति कैसा है’ यह कोई नहीं देखता, सभी की दृष्टि ‘उसके पास क्या है’ पर केंद्रित हो गयी है। सभी का दृष्टिकोण व्यवसायिक हो गया है। संतोष को अकर्मण्यता कहा जाने लगा है । ईमानदारी, कर्त्तव्यनिष्ठा और श्रम आज जैसे मूर्खता के पर्यायवाची बन गए हों; समाज-सेवा पाखंड में परिणत हो गई हो । स्वाधीनता संग्राम की अवधि में विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए हमारे जननायक जहां अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को सन्नद्ध रहते थे, वहीं स्वाधीन भारत के नेता देश का सब कुछ हड़प लेने को कटिबद्ध हैं तथा अफ़सरों को तो जैसे पद के रूप में राष्ट्र और जनता को दोनों हाथों से लूटने का लाइसेंस (अनुज्ञापन ) ही मिल गया हो | हवालों और घोटालों के रूप में इन महामहिमों की यशोगाथा हम आए दिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, दूरदर्शन पर देखते – सुनते हैं।
सामाजिक स्तर पर भ्रष्टाचार का मूल कारण व्यक्तिवाद है । लोगों में विलासिता की होड़ अपने भौतिक स्तर को ऊंचा, और ऊंचा उठाने की अत्यधिक लालसा तथा इन सबके लिए जल्दी से जल्दी अधिकाधिक धन बटोर लेने की हवस ने समाज में भ्रष्टाचार को फैलाया है । संस्थापित जीवन मूल्यों और आदर्शों के अस्वीकार और बहिष्कार से यह बेरोक-टोक बढ़ रहा है।
बड़ी विडंबना है कि भ्रष्टाचार पर कानून से अंकुश नहीं लग पा रहा है, क्योंकि कानून ही उसके समक्ष नत्मस्तक हो जाता है, न्याय बिक जाता है। समाज की अतिरंजित भौतिकवादी सोच को बदलकर, धन को जीवन का साध्य नहीं, साधन मानकर और अध्यात्म को स्वीकार करके ही भ्रष्टाचार नियंत्रण किया जा सकता है। जिस आस्तिकता को विज्ञान ने नकार दिया है, उसे पुनः स्वीकारना होगा, धर्म की शरण में जाना होगा। धर्म मानवता है, मानवीय संवेदनाओं और जीवन मूल्यों के स्वीकार और अंगीकार का नाम है। धर्म सांसारिक भोगों को नकारने या त्यागने का परामर्श नहीं देता, क्योंकि मनुष्य- मात्र के लिए यह संभव है भी नहीं। वह भोग की अनुमति तो देता है, किंतु त्याग के साथ, सब्र संतोष के साथ :
बिना संतोख नही कोऊ राजै ॥
सुपन मनोरथ ब्रिथे सभ काजै ॥ ( पन्ना २७९ )
हमें अपने मन को काबू में करना होगा। और वासनाओं का उद्गम स्थान है। कामनाएं पूरी क्योंकि यही सभी बखेड़ों की जड़ है; समस्त कामनाओं करने से और वासनाएं उपभोग करने से ये कभी शां या तृप्त नहीं होती, अपितु बढ़ती ही जाती हैं। इन्हें तृप्त करने का प्रयास आग में घी का काम करता है:
लोभ लहिर सभि सुआनु हलकु है
हलकिओ सहि बिगारै ॥ ( पन्ना ९८३)
जब तक मनुष्य उसे हृदयहीन और मानवीय संवेदना -विहीन बनाने वाली वित्तैषणा और भोग लालसा को संयत नहीं करेगा, उन पर अंकुश लगाने का प्रयास नहीं करेगा और संतोष करना नहीं सीखेगा तक भ्रष्टाचार पर नियंत्रण सम्भव नहीं है। भौतिकवाद द्वारा रोपा गया और खाद-पानी देकर बढ़ाया गया ज़हरीले फलों से लदा भ्रष्टाचार का यह विशाल वृक्ष अध्यात्म के कुल्हाड़े से ही काटा जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर न्यायपालिका की भी निष्पक्ष और कारगर भूमिका होनी चाहिए। दंडविधान भी कठोर होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि संयुक्त राष्ट्र संघ और भी शक्ति – सम्पन्न होगा तभी वह विश्व स्तर पर व्याप्त तस्करी, आतंकवाद, हथियारों की होड़ आदि पर अंकुश लगा सकता है।