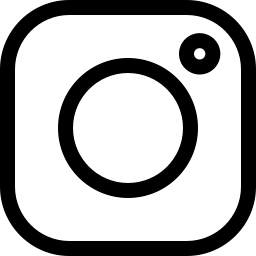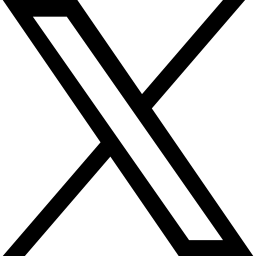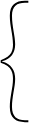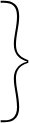– डॉ. इंदरजीत सिंघ गोगोआणी*
कबीर मानस जनमु दुलंभु है होइ न बार बार ॥
जिउ बन फल पाके भुइ गिरहि बहुरि न लागहि डार ॥ (पन्ना १३६६ )
मनुष्य का जन्म बहुत कीमती है, परंतु कीमत का एहसास ज्ञान के बिना नहीं हो सकता ।
सतिगुरु ने बार-बार मानवता को सचेत किया है :
फिरत फिरत बहुते जुग हारिओ मानस देह लही ॥
( पन्ना ६३१)
अब यदि सोए हुए विचार जागें तो ही दैवी ज्ञान से लाभ ले सकते हैं या इस तरह कहें कि मनुष्य ज्ञान वाले मार्ग पर चले तो ही लाभ ले सकता है ।
इसी तरह लोक साहित्य में सरल उदाहरण देकर भी मानवता को समझाया है कि किसी चरवाहे के बच्चे कीमती हीरे को पत्थर समझ कर बच्चों वाले खेल खेलते रहे या एक लकड़हारा अज्ञानता में ही चंदन की लकड़ियां काट-काट कर बाज़ार में ईंधन के भाव बेचता रहा । इस तरह की लोक-कथाएं वास्तव में मन के तल पर सोए हुए मनुष्य को जगाने और आत्म-चिंतन के लिए प्रेि करने का ही ढंग हैं।
वैसे व्यवहारिक जीवन में विचरण करता हुआ आम मानव अपने आप के बारे में इतना लापरवाह होता है कि वह परमेश्वर की बख़्शी रहमत की कीमत नहीं जानता। जब कहीं प्राकृतिक रूप से थोड़ा-सा भी नुक्स पड़ जाए तो शरीर को चलता रखने के लिए एक-एक अंग की कीमत लाखों में अदा करनी पड़ती है। समझदार लोगों का कथन है कि नज़र की कीमत नेत्रहीन से पूछो; पैरों की कीमत पैरों से अपाहिज से पूछो; हाथों की कीमत हाथ गंवा चुके से पूछो। कम खाने का फायदा एक देर से जागने वाला मोटा व्यक्ति ही बता सकता है।
इस संसार के मनुष्यों की लापरवाही से कुर्बान जाएं कि यदि इन्होंने मशीनरी में तेल भरवाना हो, तो ये लोग गाड़ी की औसत से लेकर इंजन के फायदे – नुकसान तक पूरे फिक्रमंद हैं, परंतु दूसरी तरफ शरीर रूपी इंजन में पदार्थ डालने हों तो बहुसंख्यक लोग हर गलत वस्तु, तरल, ठोस, नशा आदि बिना सोचे- विचारे पेट में भरते जाते हैं ।
यह धरती का सत्य है कि ज्यादातर बीमारियां मानव लापरवाही में सहेजता है और इसकी सांसारिक रसों की गुलाम हुई छोटी-सी जीभ कई बार जल्दी ही कब्र खोद देती है । उस समय इसको कीमती जीवन का देर से एहसास होता है ।
वर्तमान समय में देखें तो सड़कों पर चलती अंधाधुंध तेज़ रफ़्तार गाड़ियां, छोटे-छोटे बच्चों के हाथ में सौंपी मशीनरी, एक-दूसरे को पछाड़ आगे निकलने की लालसा मोबाइल का दुरुपयोग, रोज़ाना सड़कों पर बढ़ रही दुर्घटनाएं, जगह-जगह कुरलाते इंसान, मुश्किलें, रिश्तों का विलाप आदि मानवता के लिए खतरे की घंटी हैं। मानव को मंज़िलों पर पहुंचाने वाली सड़कें कत्लगाह बनती जा रही हैं। इसके अलावा नई तरह के शौक– नशों से लेकर आवारागर्दी तक और फैशन-परस्ती से लेकर नैतिक जीवन-मूल्यों के बिगाड़ तक परिणाम देखें तो मानवता नापाक बहाव में बह रही है। बहुसंख्यक तन और मन खतरनाक रोगों की भेंट चढ़ गए हैं।
प्रश्न है कि क्या मानव जागेगा और दूसरों को जगाएगा?
इसका उत्तर यह है कि मानव जगे भी हैं और जगा भी रहे हैं, परंतु यह संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है। यदि यह संख्या स्वयं से शुरू की जाए तो कोई गंभीर मसला ही नहीं है ।
अब तत्वसार भक्त कबीर जी के सलोक में दर्ज है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, जो बार-बार प्राप्त नहीं होता। जैसे वन में फल पक कर धरती पर गिरते हैं, तो फिर वे दोबारा पेड़ के साथ नहीं लग सकते अर्थात् उनकी जीवन लीला खत्म हो जाती है, इसी तरह यदि मानव अपने निजी जीवन और धर्म कर्म के प्रति जाग जाए तो यही धरती स्वर्ग बन जाएगी और उसकी यह मानव जीवन रूपी यात्रा सफल मानी जाएगी।
व्यवहारिक पक्ष के साथ अब आध्यात्मिक पक्ष भी है, जो “भई परापति मानुख देहुरीआ ॥ गोबिंद मिलण की इह तेरी बरीआ ” का सत्य उपदेश है। सिक्ख फलसफे के अनुसार समूची मानवता को अपने फर्मों के प्रति सचेत किया है कि प्रभु -मिलाप का यही समय है। पंचम पातशाह जी फरमान करते हैं कि चौरासी लाख योनियों में से मनुष्य जन्म उत्तम जीवन है और यदि फिर भी प्रभु-मिलाप से विहीन रह गया तो जन्म-मरण का दुख भोगता रहेगा :
लख चउरासीह जोनि सबाई ॥
माणस कउ प्रभि दीई वडिआई ॥
इसु पउड़ी ते जो नरु चूकै
सो आइ जाइ दुखु पाइदा ॥ ( पन्ना १०७५)
संसार से लेकर निरंकार तक सब भले कार्य मनुष्य जन्म में ही हो सकते हैं। आओ, इस मनुष्य जन्म की कीमत पहचानें!
सिक्ख भाईचारे को एकजुट करना भाई गुरदास जी की वारों के मुख्य सरोकारों में से है। वैदिक मत में ब्राह्मण द्वारा दी जाने वाली विद्या भी जाति पर आधारित थी । उसने कथित नीच श्रेणियों को अशिक्षित रखने के लिए उनको शिक्षा से वंचित किया हुआ था। श्री गुरु नानक देव जी ने ब्राह्मण के इस भेदभावी व्यवहार को देखते हुए गोपाल पुरोहित से विद्या प्राप्त करने से इनकार कर दिया था। श्री गुरु नानक देव जी ने ‘दखणी ओअंकार’ बाणी में ब्राह्मण को संबोधित होकर कहा कि असली अध्यापक वह है, जो स्वाभाविक विद्या में विचरण करे अर्थात् विद्या देते समय पक्षपात से ग्रसित न हो । मन के पीछे चलने वाला व्यक्ति विद्या बेचता है। वह विद्या को हर अमीर-गरीब तक नहीं पहुंचाता, बल्कि भौतिक लाभ हेतु धनवान वर्ग को ही शिक्षित करता है :
पाधा पड़िआ आखीऐ बिदिआ बिचरै सहजि सुभाइ ॥
बिदिआ सोधै ततु है राम नाम लिव लाइ ॥
मनमुखु बिदिओ बिक्रदा बिखु खटे बिखु खाइ ॥
( पन्ना ९३७)
इस व्यवहार के विपरीत भाई गुरदास जी कहते हैं कि ज्ञानवान गुरमुख वह है, जो सारे संसार को बिना किसी भेदभाव के ज्ञान प्रदान करता है, क्योंकि उसका जीवन सत्य पर टिका है। वह संतोषी है, लालची नहीं, कामी-क्रोधी नहीं। शुद्ध अंत:करण वाला वह आदर्श मानव ( जाति आदि के) अभिमान से मुक्त है। वह वैर – विरोध से मुक्त है। वह चार वर्णों को धर्म का उपदेश देता है । इस तरह भाई गुरदास जी द्वारा बताया गया गुरमुख स्वयं ज्ञानवान होता है और जगत में बिना किसी भेदभाव, स्वार्थ और लालच के ज्ञान बांटता है :
गुरमुख पंडित होइ जगु परबोधीऐ ।
गुरमुखि आy गवाइ अंदरु सोधीऐ ।
गुरमुखि सतु संतोखु न कामु करोधीऐ ।
गुरमुखि है निरवैरु न वैर विरोधीऐ ।
चहु वरना उपदेसु सहजि समोधीऐ ।
धनु जणेदी माउ जोधा जोधीऐ ॥ (वार १९:१८ )
गुरु पर अटूट विश्वास : सिक्ख की जीवन-युक्ति उसके अपने यत्नों का फल नहीं, बल्कि गुरु द्वारा जगत में प्रकट हुई है। यह युक्ति उसे गुरु कृपा के बिना प्राप्त नहीं हो सकती। ज़रूरी है कि सिक्ख का अपने गुरु पर अटूट विश्वास हो । सिक्ख को यह यकीन होना ज़रूरी है कि सच्चे गुरु जैसा बख़्शिशें करने वाला कोई माता-पिता या देवी – देवता नहीं हो सकता :
सतिगुरु तुलि न मिहरवान मात पिता न देव सबाए ।
डिठे सभे ठोकि वजाए ॥ ( वार ३९:२० )
सति और नाम का सौदा एक ही स्थान से प्राप्त हो सकता है। दर-दर की ठोकरें खाने वाला मनुष्य वह वस्तु प्राप्त नहीं कर सकता, जिससे पूर्ण विश्वस्त मानव को पूरा लाभ मिलता है:
सउदा इकतु हटि सबदि विसाहीऐ ।
पूरा पूरे वटि कि आखि सलाहीऐ । ( वार ३:६ )
सच्चे गुरु की शरण में गए बिना जीवन जीने की सही विधि समझ नहीं आती :
सतिगुर बिना न सोझी पाई ॥ (वार १:९)
क्योंकि गुरु के बिना आशंका दूर नहीं होती
सतिगुर बिना न सहसा जावै ॥ (वार १:१०)
भाई गुरदास जी कहते हैं कि गुरमुख-पंथ में गुरु की शिक्षा ही सिक्ख-साधक की माता है अर्थात् जीवन-युक्ति का दान देने वाली गुरमति है और सब गुणों के ऊपर शोभित मुक्ति-प्रदाता सद्गुण संतोष पिता है। धीरज और धर्म दो भाई हैं, जो हर संकट में उसकी बाजू बनते हैं । जप-तप और जत-सत पुत्र हैं जो गुरमति के धारक संतोषी, धीरजवान और धर्मी गुरमुख के घर जन्म लेते हैं अर्थात् उसकी जीवन – युक्ति में से खुद प्रकट होते हैं। भारत के सनातनवादी पंथों में जप-तप और ब्रह्मचर्य माता-पिता की पदवी पर शोभित थे। भाई साहिब के ज्ञान – चमत्कार ने उनको साधना में से उत्पन्न होने वाला पुत्र बना दिया अर्थात् उनको साधना का अंतिम निशाना नहीं रहने दिया । इस कथन को समझने की ज़रूरत है। सिक्ख पंथ में त्यागवाद नहीं एकांत में जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि एकांतवास छोड़ कर गुरमुखों की संगत में जाकर ध्यान लगाने की प्रेरणा है। त्यागवादी ने ब्रह्मचर्य और जप-तप साध कर आध्यात्मिक ज्ञान, संतोष, धीरज, धर्म आदि गुण प्राप्त करने हैं। गुरमुख ने साधसंगत से ज्ञान प्राप्त किया, सेवा से संतोष लिया, लोक में विचरण कर धीरज अर्थात् सहनशीलता प्राप्त कर ली । सत् – संतोष आदि गुण धारण करना ही उसका धर्म था । साधसंगत द्वारा नाम का जप रूप पुत्र प्राप्त हुआ और मानवता की सेवा से मेहनत रूपी तप मिल गया। निज नारी के स्नेह से वास्तविक ब्रह्मचर्य मिल गया। भाई गुरदास जी सिक्ख विचारधारा का निरालापन बता रहे हैं। इससे ‘होरिंओं गंग वहाईए’ का प्रमाण प्रत्यक्ष हो जाता है। जो प्राप्तियां भारतीय साधना की शिखर थीं, गुरमति में आसानी से प्राप्त होने वाली गौण वस्तुएं हो गईं। गुरमति विचारधारा में जप, तप, ब्रह्मचर्य छोटे हो गए। गुरु का ज्ञान और संतोष आदि सद्गुण ऊंचाइयों पर सुशोभित हो गए । भाई साहिब का महत्वपूर्ण वर्णन है :
गुरमति माता मति है
पिता संतोख मोख पदु पाइआ ।
धीरजु धरमु भिराव दुइ
जपु तपु जतु सतु पुत जणाइआ । ( वार ६ : ५ )
इसलिए सिक्ख की जीवन – युक्ति में गुरु पर मुकम्मल विश्वास अनिवार्य है। वह अस्थिर सिक्ख है, जो गुरु- पुत्र न होते हुए श्री गुरु अंगद देव जी ( भाई लहिणा जी ) को गुरुआई सौंपने पर, श्री गुरु अमरदास जी द्वारा श्री गुरु अंगद देव जी की सेवा करने और श्री गुरु हरिगोबिंद साहिब जी के शस्त्रधारी व्यवहार पर संशय – ग्रसित हो जाए । आदर्श गुरमुख सिक्ख बनने के लिए गुरदेव पर पूर्ण भरोसा ज़रूरी है। चाहे गुरु का विचित्र कौतुक देखकर बहुत से डर जाते हैं, परंतु बख़्शिश-प्राप्त पूर्ण और सम्मुख सिक्ख अचल रहते हैं :
–जे गुर सांगि वरतदा सिखु सिदकु न हारे ॥ (वार ३५:२० )
— सांगै अंदरि साबते से विरले बंदे ॥ (वार ३५ : २१)
–सांगै अंदरि साबता जिसु गुरू सहाए ॥ (वार ३५:२३)
भाई गुरदास जी ने सिक्ख को उन नकली गुरुओं से भी सावधान किया है, जिनमें गुरु वाले गुण तो कोई नहीं परंतु उनके आसन सच्चे गुरु से भी शोभनीय एवं संवारे हुए हैं :
विणु गुणु गुरू सदाइदे ओइ खोटे मठे || ( वार ३६: ९ )
एक अकाल पुरख पर विश्वास मानव-जीवन का सबसे बड़ा दुखांत है और उसका सर्वोपरि कुकृत्य है परमेश्वर के नाम पर दूसरों के साथ वैर-विरोध करना । वह एक ही दैवी सत्ता, जिसने सारी मानवता को जोड़ना था, जिसने सभी जीवों में एक ही जीवन की विद्यमानता का मानव को एहसास करवाना था, जो विश्वस्त की सभी अच्छाइयों का मूल है, उसके नाम पर विवाद हों, मानवता के लिए इससे शर्मनाक कोई और कार्य नहीं हो सकता। श्री गुरु नानक देव जी ने ‘जपु’ बाणी में “सभना जीआ का इकु दाता सो मै विसरि न जाई ॥” कहकर मानवता को केवल परमेश्वर के सिमरन के साथ जोड़ा था, जिसमें सभी जीवों का साझा पिता होने की योग्यता है; जो किसी संप्रदाय, जाति, कुल, वर्ण, पंथ, देश आदि सीमाओं के बंधन में नहीं है या राष्ट्रीय ईश्वर नहीं है । परिपूर्ण गुरु साहिबान द्वारा वर्णित गुरमुख-पंथ का परमेश्वर संकीर्ण, संकुचित और सीमित नहीं। उसमें सभी इष्टों के स्वरूप और सर्वनाम विलीन हो सकने की केवल संभावना ही नहीं, बल्कि विलीन रहते हैं। यहां तक कि नास्तिक शून्यवाद भी उसमें स्थापित हो जाता है- “आसति नासति एको नाउ” हो जाता है अर्थात् आस्तिकता और नास्तिकता उसमें दोनों समरूप हो जाते हैं। सिक्ख – चिंतन का प्रसार कर ब्रह्म संबंधी सांप्रदायिक संकीर्णता दूर करने के लिए भाई गुरदास जी ने सिक्ख की जीवन-युक्ति के केंद्र-बिंदु वाहिगुरु के स्वरूप में विष्णु, हरि, गोबिंद और राम एक रूप कर दिए अर्थात् संकुचित राष्ट्रीय देवताओं को सर्वव्यापक, सर्वमान्य, सर्वशक्तिमान प्रभु में अभेद कर दिया। गुरमुख जब परमेश्वर का नाम जपता है, तो उसकी व्यापकता का विचार वह कभी नहीं त्यागता । हालांकि भाई साहिब भली-भांति परिचित थे कि ‘वाहिगुरु’ नाम वाह + हे + गुरु इन तीन पदों का सुमेल है, परंतु ब्रह्म की एक सत्ता स्थापित करने के प्रयोजन से उन्होंने वाहिगुरु पद की बनावट में विष्णु, हरि, गोबिंद और राम को विलीन कर दिया । उन्होंने कहा कि ये चार तो चार युगों के परिवर्तनशील खत्म हो जाने वाले ईश्वर थे। श्री गुरु नानक देव जी ने कृपा कर परमेश्वर के विभिन्न नाम सर्वोच्च ब्रह्म ( पंचायण ) में स्थापित कर दिए हैं। छोटे- बड़े पैगंबरों के स्थान पर ऐसे अनाम प्रभु का चिंतन दे दिया है, जिसे ज्ञान – मूल मान कर धन्य-धन्य ही कहा जा सकता है। परमेश्वर को सारी मानवता का अद्भुत मार्गदर्शक कह सकते हैं, किसी नाम में बांध नहीं सकते। जिस प्रभु को अज्ञानी लोगों ने अनेकता में बांट दिया था, उसकी अनेकता को एकता में अभेद कर दिया है। भाई गुरदास जी कहते हैं :
सतजुग सतिगुर वासदेव
वा विना नामु जपावै ।
दुआरि सतिगुर हरीकिशन
हाहा हरि हरि नामु जपावै।
तेते सतिगुर राम जी
रारा राम जपे सुखु पावै ।
कलिजुग नानक गुर गोबिंद
गागा गोबिंद नामु अलावै ।
चारे जागे चहु जुगी
पंचाइण विचि जाइ समावै ।
चारो अछर इकु कर वाहगुरू जपु मंत्र जपावै ।
जहा ते उपजिआ फिरि तहा समावै ॥ ( वार १ : ४९ )
यहां यह भी स्पष्ट कर दिया जाए कि इस पद के मूल भाव, उद्देश्य और व्यापक सिद्धांत को जाने बिना कुछ सिक्ख अनुचित ढंग से भाई साहिब को हिंदूवादी कहकर उनकी सिक्खी – निष्ठा संबंधी भ्रम पैदा कर रहे हैं, जबकि भाई साहिब का उद्देश्य अवतारों और देवताओं के साथ जोड़ना नहीं, बल्कि सब अवतारों को भेजने वाले देवानदेव अकाल पुरख के साथ जोड़ना है; ब्रह्म से संबंधित संकीर्णता को तोड़ना है। भाई साहिब की वारें सनातनी विचारधारा, अवतारवाद, देव- पूजा और धार्मिक कर्मकांड का पुरज़ोर विरोध करती हैं। उनकी सातवीं वार पुरातन सनातनवाद की समूची व्यवस्था को अस्वीकार कर गुरमुख ने कैसे युक्तिसंगत कर्म ग्रहण किए हैं, इसका विस्तृत विवरण है। इस वार की तीसरी पउड़ी में भाई साहिब कहते हैं कि गुरमुख ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिलोक, वेद, त्रिगुण, त्रिकाल, जन्म-मरण, तीन ताप, तीन वर्ण जीवन की तीन अवस्थाओं, प्रणायाम, तिकुटी, त्रिवेणी सबको जीत कर अपने आपको सबसे ऊपर स्थापित किया है :
ब्रहमा बिसनु महेसु
लोक वेद गुण गिआन लंघाए ।
भूत भविखहु वरतमानु
आदि मधि जिणि अंति सिधाए ।
मन बच करम इकत्र करि
जंमण मरण जीवण जिणि आए।
आधि बिआधि उपाधि साधि
सुरग मिरत पाताल निवाए ।
उतमु मधम नीच साधि
बालक जोबन बिरधि जिणाए ।
इड़ा पिंगुला सुखमना
त्रिकुटी लघि त्रिबेणी न्हाए ।
गुरमुख इकु मनि इकु धिआए ॥ ( वार ७:३)
द्वैत-अद्वैत का निर्णय धार्मिक समुदाय के धर्म-शास्त्र की प्रमुख समस्या है। अगर द्वैतवाद मान लिया जाए, तो मानवता में अतर्निहित संबंध कैसे स्थापित हो ? सारे स्थूल पसारे को एक इकाई कैसे माना जाए? एक ही सर्वशक्तिमान परम सत्ता का अस्तित्व कैसे सिद्ध किया जाए? अगर अद्वैत मान लें तो की बदी का मूल एक कैसे माना जाए ? भौतिक जगत को परिभाषित कैसे किया जाए? अद्वैत के अस्तित्व में साधक साधना किसकी करे? ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिनका समाधान धर्म – शास्त्रियों के लिए कठिन कार्य है। शुद्ध इसलाम में अस्तित्व की अनेकता का विधान देखा जा सकता है। जहां ईश्वर ने सब कुछ बनाया तो है, मगर उसमें से न कुछ निकला है, न उसमें कुछ विलीन हो सकता है। हर चीज़ का उत्पन्न होने का स्रोत भिन्न है। जीव एक योनि में से दूसरी योनि में नहीं जा सकता । फरिश्ता अग्नि से बना है और मानव की सृजना मिट्टी से है। मानव को धर्म के रास्ते पर अल्लाह चलाता है, परंतु बुराई के रास्ते पर शैतान डालता है। मोमिन और काफिर एकरूप नहीं माने जा सकते, क्योंकि मोमिन अल्लाह के रास्ते पर है, जबकि काफिर ने शैतान का मार्ग अपनाया है। दूसरी तरफ इसलाम की साधना में से ही प्रकट हुए सूफी महात्मा थे, जिनका चिंतन अस्तित्व की एकता पर टिका होने के कारण ज्यादातर सूफी ‘वहदतुल वजूद’ के प्रबल समर्थक थे । उनका नारा पूर्ण अद्वैत था। भारतीय दर्शन चाहे बहुदेववादी और बहुअवतारवादी सगुणता – परस्त होने के कारण द्वैतवादी प्रतीत होता है, लेकिन यहां के वैदिक अवैदिक मत के चिंतकों ने इसको अद्वैतवाद की शिखर पर ही शोभित किया, चाहे वे धर्म-चिंतक स्थायी अस्तित्व का विरोध करने वाले शून्यवादी ही क्यों न हों। शून्यता भी वास्तविकता में अस्तित्व ही थी, जिसका विकास अद्वैत – चिंतन में से ही होता है, इसलिए शून्यता जो कभी ब्रह्म के अस्तित्व से संबंधित नकारात्मक सिद्धांत प्रतीत होता था, धीरे – धीरे खुद भी अद्वैत ब्रह्म का ही रूप धारण कर गई। गुरबाणी के निम्नांकित वचनों से यह स्पष्ट है
– आपहि सुन आपहि सुख आसन ॥
आपहि सुनत आप ही जासन ॥
— सरगुन निरगुन निरंकार सुन ( पन्ना २५० )
समाधी आपि ॥
आपन कीआ नानका आपे ही फिरि जापि ॥१॥
( पन्ना २९० )
– सुनहु चंदु सूरजु गैणारे ॥
तिस की जोति त्रिभवण सारे ॥
सुने अलख अपार निरालमु सुने ताड़ी लाइदा ॥ (पन्ना १०३७)
द्वैत-अद्वैत से संबंधित सिक्ख पंथ के परंपरागत ज्ञानी, विशेष तौर पर निर्मल भेस के विद्वान बहुत स्पष्ट थे कि गुरमति अद्वैतवाद आध्यात्मिक चिंतन है । जो लोग द्वैत-अद्वैत के भेद को सूक्ष्मता के साथ नहीं जानते थे, उन्होंने इसी अद्वैत निष्ठा के कारण उनको वेद- परस्त कहकर सिक्खी विचारधारा से दूर बताया। इसमें कोई संदेह नहीं कि गुरमुख-पंथ (सिक्ख पंथ ) में सूफी साधना की आध्यात्मि मंजिल अहंवादी ‘अनहलहक’ और वेदांत के ‘अहम ब्रहम असमि’ को कम से कम स्थूल रूप में कोई स्थान नहीं दिया गया, बल्कि हर अवस्था में साधक सेवक है और अकाल पुरख उसका मालिक है । परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है और सेवक उसके चरणों में है। प्रभु सर्व-भांति निर्मल है, परंतु सेवक हर पक्ष से अपवित्र है। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि “ताही ते उपजि सभि ताहि महि समाहिगे” का विधान गुरमति की आत्मा है। निराकार परमेश्वर खुद आकारधारी होता है अपने आप में से ‘दूई कुदरति’ बनाता है; अपने आप में से ही जीव बनाता है; जीव उसी में विचरण करता है, उससे बाहर कभी नहीं जा सकता और अंत में “जह ते उपजी तह मिली” की अवस्था प्राप्त करता है । जो कुदरत कादर ने बनाई है, उसमें वह विराजमान है। उसने कुदरत को अपने से भिन्न नहीं रखा कि इसे स्वतंत्र छोड़कर स्वयं सातवें आकाश पर या किसी तथाकथित विशेष स्वर्ग आदि में जा बैठा हो। वह जगत में बैठा ही नहीं बल्कि जगत उसका विस्तार होने के कारण वह खुद ही नाना रूपों में विचरण कर रहा है और रचना से अभिन्न है। उसकी अपनी रचाई लीला के कारण स्वरूपधारी जीवों को अपने अलग वजूद का भ्रामिक एहसास होने लगता है, क्योंकि इस अलग वजूद का एहसास जागृत हुए बिना ब्रह्म के नाना स्वरूप धारण करने के खेल का प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता। अगर वह यह भ्रम उत्पन्न नहीं करता, तो उसके नाना स्वरूपों में क्रियाशील होने की संभावना नहीं हो सकती थी । सुखमनी साहिब की इक्कीसवीं असटपदी में इस विचार की विस्तृत चर्चा है । हम यहां अपने विचार की प्रमाणिकता के लिए संक्षिप्त प्रमाण प्रस्तुत करते हैं
जब होवत प्रभ केवल धनी ॥
तब बंध मुकति कहु किस कउ गनी ॥
जब एकहि हरि अगम अपार ॥
तब नरक सुरंग कहु कउन अउतार ॥
जब निरगुण प्रभु सहज सुभाइ ॥
तब सिव सकति कहहु कित ठाइ ॥
जब आपहि आप अपनी जोति धरै ॥
तब कवन निरु कवन कत डरै॥ ( पन्ना २९१ )
यहां यह भी जान लें कि द्वैत-अद्वैत दोनों ही दिव्य हैं, क्योंकि द्वैत भी ईश्वर -कृत हैं । अंतर यह है कि द्वैत एक भ्रम है या जागतिक सत्य है, जबकि अद्वैत अंतिम सत्य है । ब्रह्म की माया में ही जीव बहुप्रकार के अस्तित्व कल्पित कर लेते हैं । अद्वैत की व्याख्या में भी बहुत अंतर है । वेदांत के अनुसार बहु-स्वरूप ही भ्रम है। गुरमति के अनुसार बहु- स्वरूप होना भ्रम नहीं, बहु- अस्तित्व होना भ्रम है। स्वरूपों की अनेकता में से एक अस्तित्व देखना, मानना और इसका अंतर्मन में मनन करना गुरमति है, मगर बहु – स्वरूप का भ्रम नष्ट करना वेदांत है ।