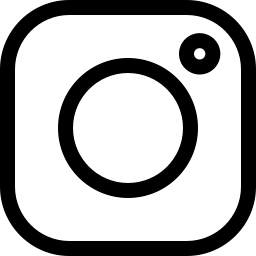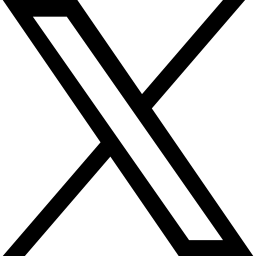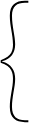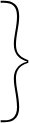गुरबाणी के शब्दों की व्याख्या करें तो गुरु साहिबान ने अभिमान (अहं, घमंड) को गंभीर रोग बताया है। हमारे भारतीय सभ्याचार में दार्शनिकों और विद्वानों द्वारा भी मानव के अंदर पाँच विकार बताए गए हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उन्होंने भी इन पाँच विकारों में से अहंकार (अभिमान) को सबसे बड़ा दर्जा दिया है। आधुनिक युग में, विज्ञान की तरक्की के साथ-साथ जब बहुत ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा किया गया तो इसमें मानव-स्वास्थ्य के प्रति भी विस्तार सहित बात हुई है। द्वितीय विश्व युद्ध के तबाहकुन परिणाम के बाद, विश्वस्तरीय संस्थाओं का गठन हुआ और मानवीय तबाही के मद्देनज़र, मानवीय विकास को प्राथमिकता दी गई।
मानवीय विकास के अंतर्गत स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राथमिकता दी गई। स्वास्थ्य संस्था का जिम्मा ‘विश्व स्वास्थ्य संस्था’ का गठन कर, उसके जिम्मे दिया गया। स्वास्थ्य को वैज्ञानिक नज़रिए से समझते हुए, संस्था ने स्वास्थ्य की व्याख्या की कि स्वस्थ होना केवल किसी तरह की बीमारी से रहित होना नहीं है, बल्कि मानव का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर पूरी तरह से स्वस्थ होना भी है।
अगर हम अपनी रोज़मर्रा की निजी ज़िंदगी में झांक कर देखें तो हम लोग किसी शारीरिक समस्या को ही बीमारी समझते हैं। अब हम लोग कुछ समय से मानसिक उलझनों और मानसिक तकलीफ़ के प्रति सजग हुए हैं। यदि सामाजिक स्वास्थ्य की बात करनी हो तो उसके बारे में हमने अभी सोचना भी शुरू नहीं किया।
स्वास्थ्य के ये तीनों पक्ष कोई अलग-अलग बाँटे हुए हिस्से नहीं हैं, बल्कि एक- दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। हम शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सभी परिचित हैं। मन की अवस्था, जैसे— उदासी और बेचैनी के प्रति हम सचेत होने लगे हैं। तीसरा पक्ष है— सामाजिक, जो कि हमारे आपसी सामाजिक रिश्तों के साथ जुड़ा हुआ है। हम देख रहे हैं कि दिन-ब-दिन यह पक्ष समाज में से कम हो रहा है या बहुत निचले स्तर पर पहुँच गया है। “हउमै दीरघ रोगु” को अगर समझना हो तो यह सामाजिक और मानसिक दोनों पक्षों के आपसी मेल में से पैदा होता है। अभिमान को साधारण शब्दों में समझें तो इसके अर्थ हैं— “केवल मैं ही खास हूं। मैं किसी अन्य को कुछ नहीं समझता।” हम इस स्थिति को जब सामाजिक घटनाक्रम में घटित होता हुआ देखते हैं तो हमारे रिश्तों में दरार आनी शुरू हो जाती है और आपस में दूरी बढ़ जाती है। अकेलेपन की हालत में बेचैनी का सामना करना पड़ता है। अकेलापन धीरे-धीरे घबराहट और अंत में उदासी की तरफ ले जाता है। इस उदासी की हालत को हम लोग आजकल अफने आस-पास घटित होता तथा बढ़ता हुआ देख रहे हैं। अब तक हमने जाना है कि इसकी जड़ में बड़ा हाथ मानव के अभिमान का है।
गुरबाणी की उपरोक्त पंक्ति का दूसरा हिस्सा है— “दारू भी इसु माहि।।” इसका अर्थ है कि इस मानसिक विकार का इलाज भी इसके अंदर ही छिपा हुआ है, मतलब, हमारे अपने अंदर ही। यह मात्र ‘मैं’ को ख़त्म करना ही नहीं है, जिस प्रकार कि प्रचार किया जाता है, बल्कि ‘मैं’ को अपने अनुकूल बनाना होता है। ‘अभिमान’ को ‘स्वाभिमान’ के रूप में लिया जाता है, जब कोई अपने आप पर अपनी काबलियत के आधार पर फख्र, मान महसूस करता है और इस फख्र, मान का मतलब है कि उसे अपने कर्म पर आधारित पहचान मिले। ऐसे में अकड़बाज होने या अपनी पहचान को लेकर हठ करने की ज़रूरत नहीं है।
गुरबाणी में एक अन्य वाक्य है— “मिठतु नीवी नानका”, जिससे मानव अपने सामाजिक रुतबे के साथ, अपनी बोल-चाल में मीठा बोले और नम्रतापूर्वक बात करे। जब बेचैनी और परेशानी की बात होती है तो इसके साथ जुड़ी दिल की अलामतों को लेकर ब्लड प्रेशर (लहू का दबाव) जैसी बीमारियाँ और दिल के दौरे की घटनाएँ रोज़ाना सुनने को मिलती हैं। बेचैनी और परेशानी से छुटकारा पाने के लिए अभिमान के सम्बंध में गुरबाणी में ही शब्द हैं— “हउमै बुझै ता दरु सूझै॥ गिआन विहूणा कथि कथि लूझै॥” अभिमान या अहंकार को दीर्घ रोग इसी लिए बताया गया है कि अभिमान में इंसान स्वास्थ्य की तीनों अवस्थाओं से पीड़ित होता है। अभिमान मानवीय रिश्तों में खलल तो डालता ही है, बल्कि शारीरिक तौर पर भी नकारा कर देता है और मन भी उदास-उदास रहता है।
अभिमान का एक इलाज ‘ज्ञान’ है, जिसके द्वारा अभिमान का अंधकार दूर किया जा सकता है। जब मानव अभिमानग्रस्त होता है तो उसे कुछ नहीं सूझता। उसको अपने हो रहे नुकसान का भी बोध नहीं होता। हमारा समाज आपस में मिल कर एक-दूसरे की मदद कर, एक-दूसरे को सहारा देकर ही आगे बढ़ सकता है। समाज का विकास मानव के इसी रवैये ने किया है। समूचे समाज को गुरबाणी की शिक्षा पर चलने की ज़रूरत है, ताकि स्वस्थ और आरोग्य समाज का निर्माण किया जा सके।
–डॉ. श्याम सुंदर दीप्ति*